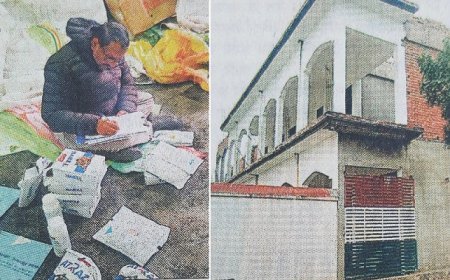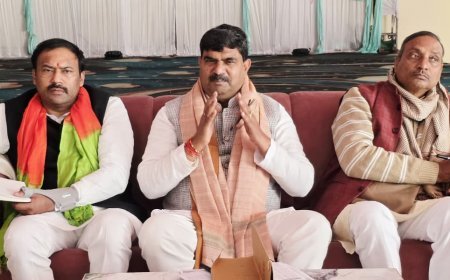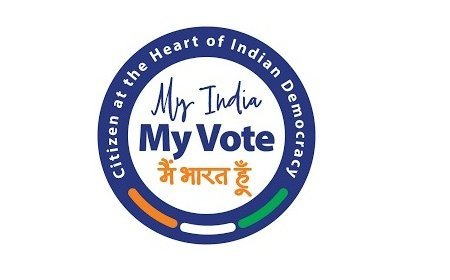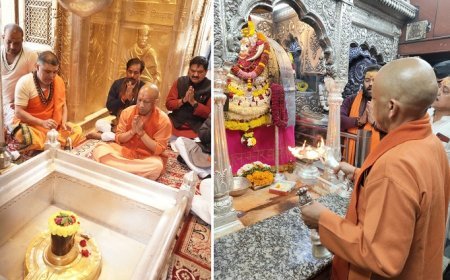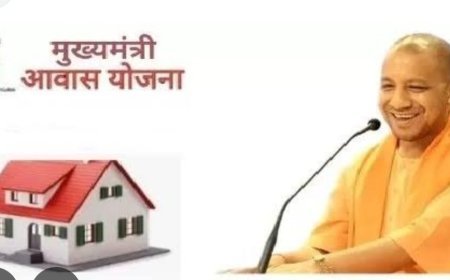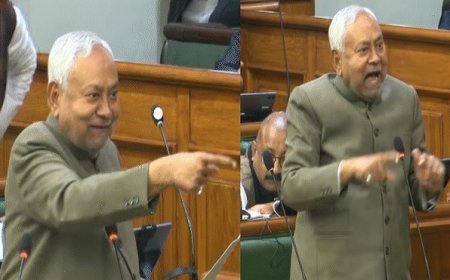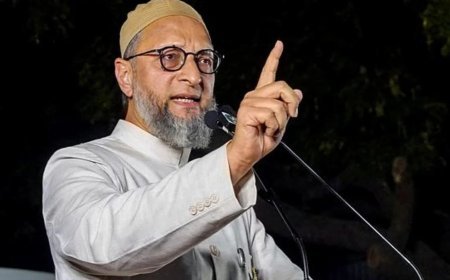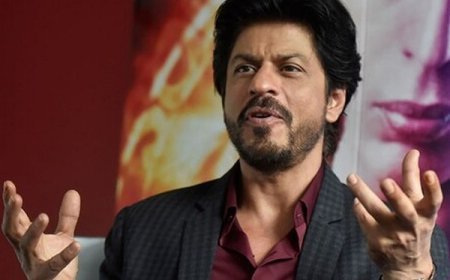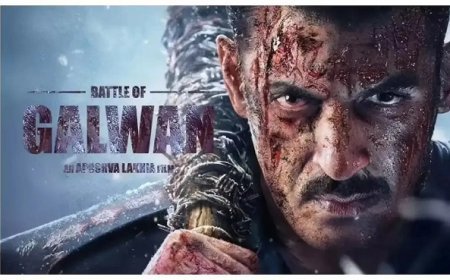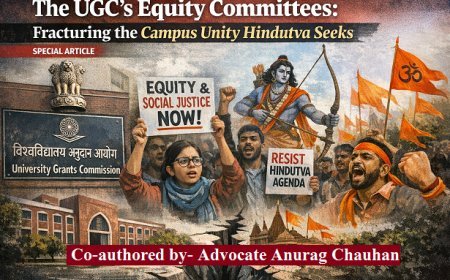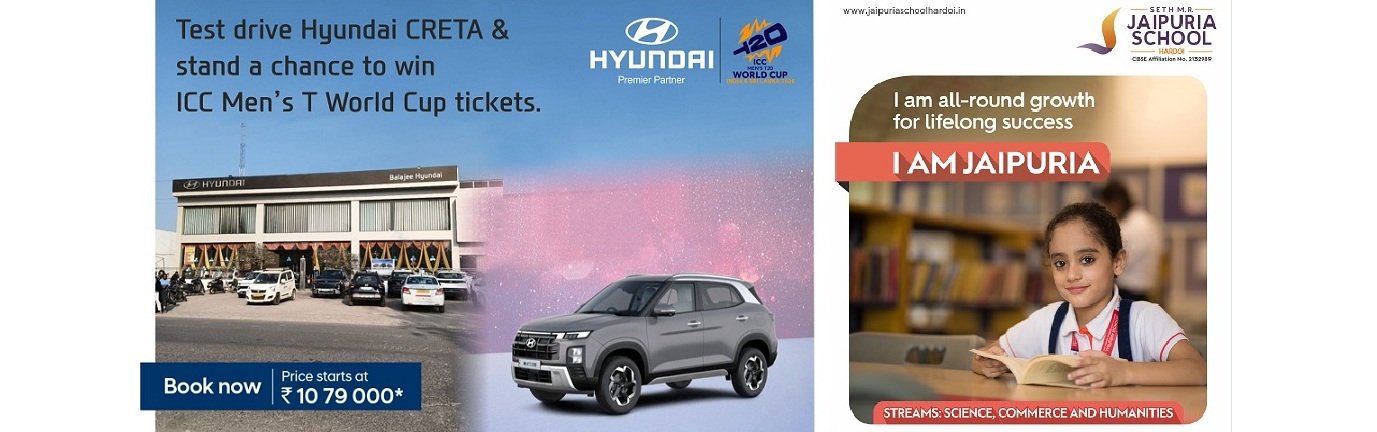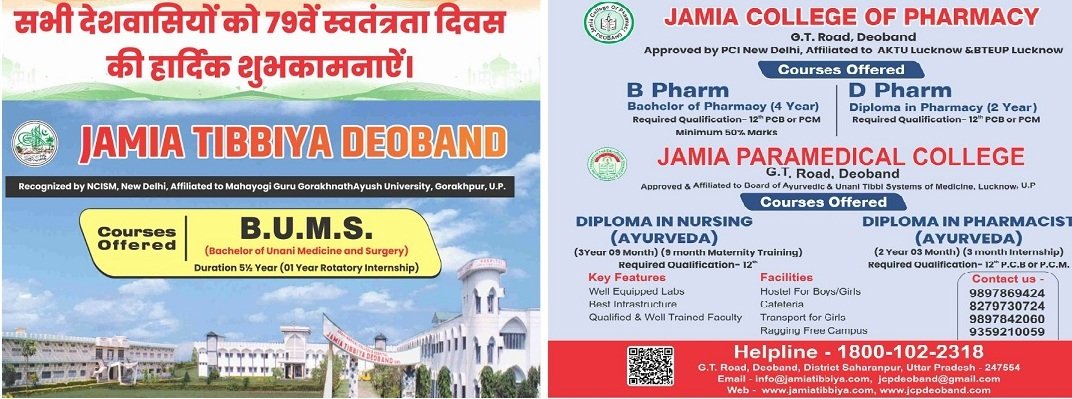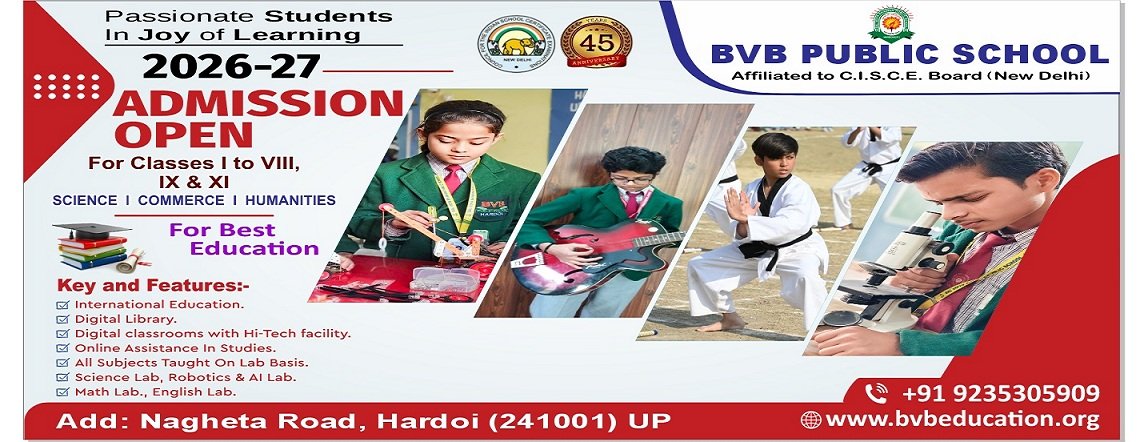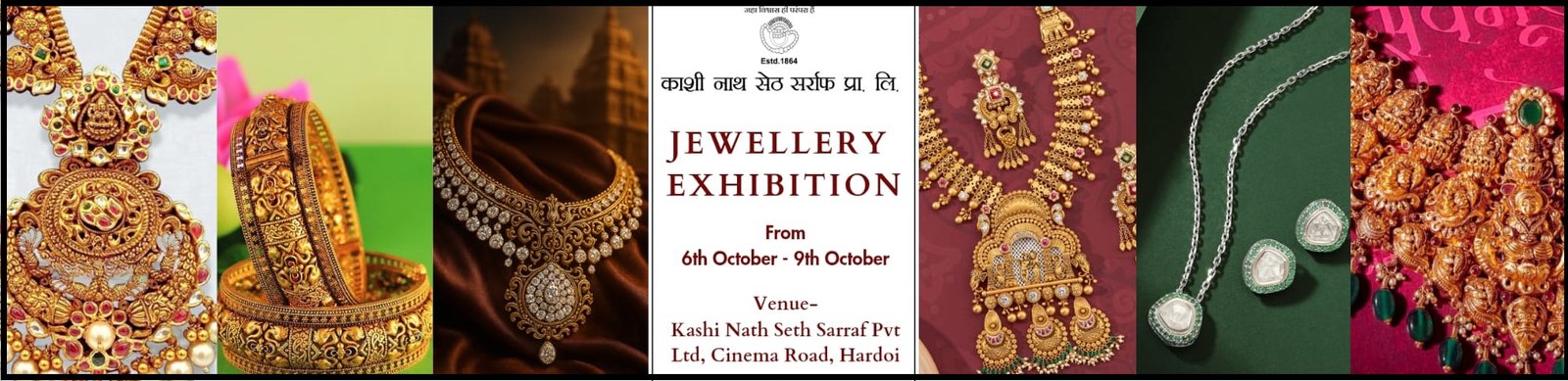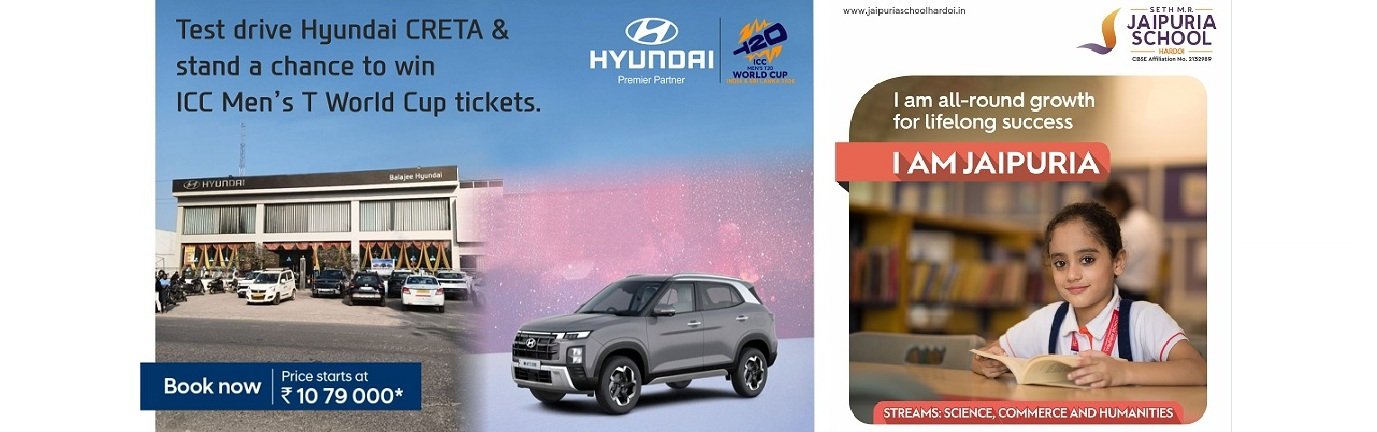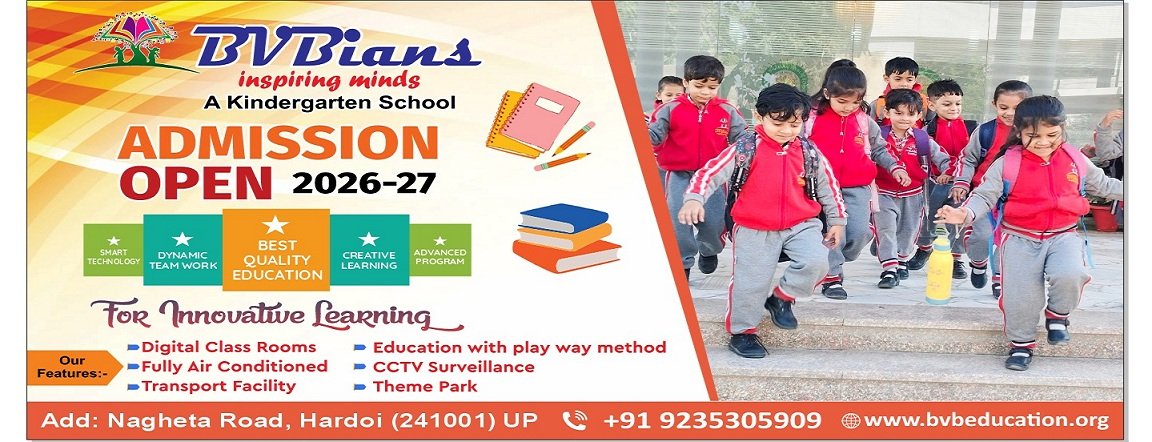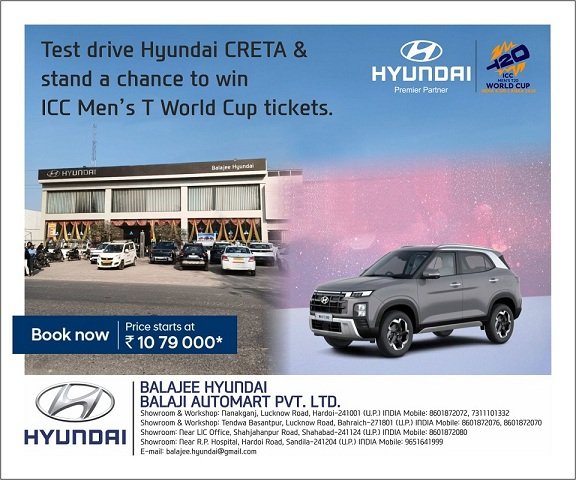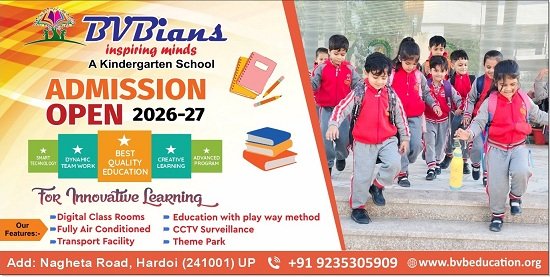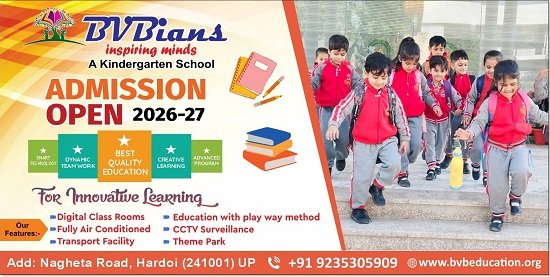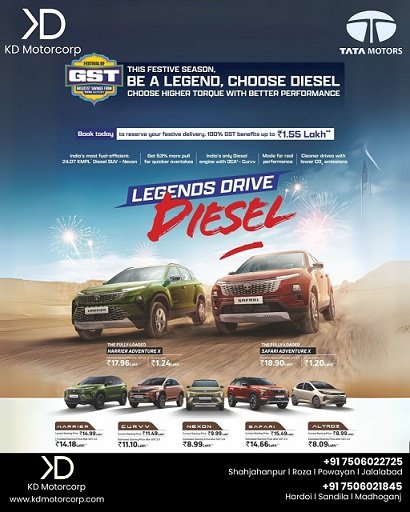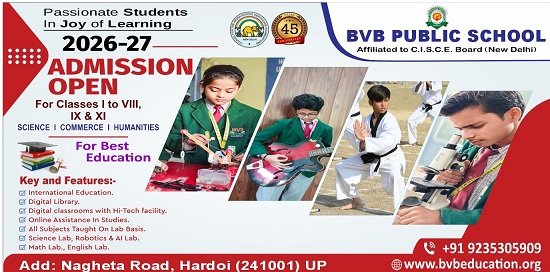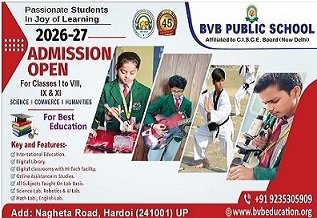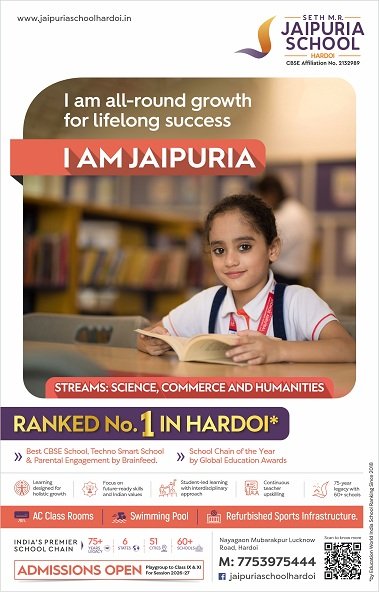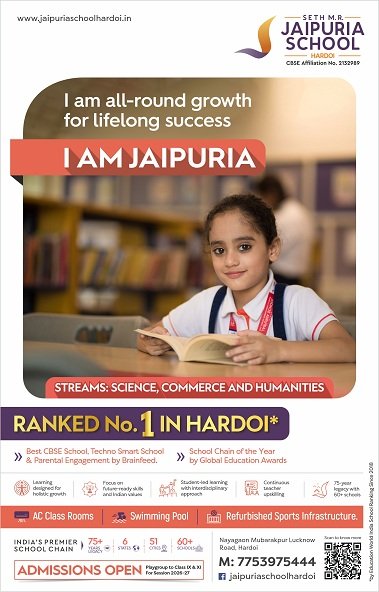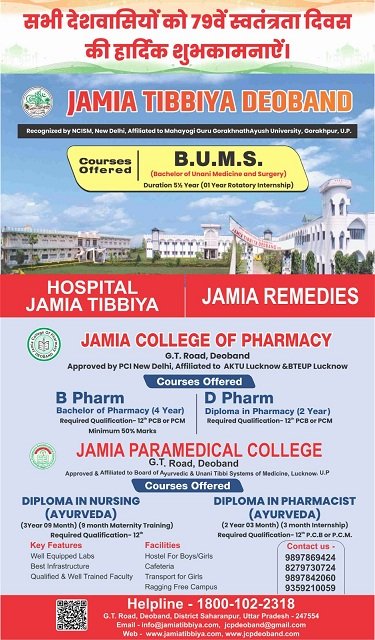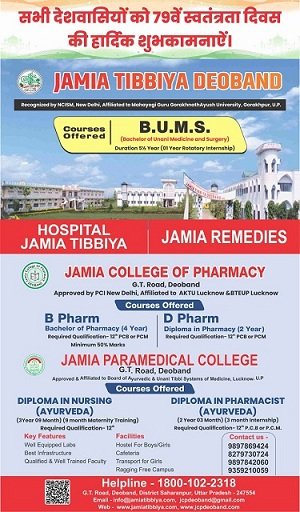विशेष लेख: चुनावी रणनीति का नया युग- कैसे मतदाता करता है फैसला ?
चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं होते, बल्कि यह मतदाताओं की सोच, मानसिकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया का दर्पण भी होते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव ....

लेखक: विक्रांत निर्मला सिंह
शोधार्थी, एनआइटी, राउरकेला
चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं होते, बल्कि यह मतदाताओं की सोच, मानसिकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया का दर्पण भी होते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणामों पर अनेक विश्लेषण उपलब्ध हैं। लेकिन इन परिणामों ने एक बार फिर इस बात पर विचार करने को मजबूर कर दिया कि मतदाता आखिर किस तरह सोचता है और अपने निर्णय तक कैसे पहुंचता है। जिस महाराष्ट्र में एक ‘तगड़ी टक्कर’ की बात कही जा रही थी, वहां अप्रत्याशित जीत और जिस झारखंड में भाजपा के लिए ‘जीत’ का दावा किया जा रहा था, वहां करारी हार। इन चुनाव परिणामों ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब न सिर्फ़ राजनीति बल्कि समाज की सामूहिक मानसिकता को समझने के लिए भी अनूठे हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मतदाता कैसे अपनी राय बनाता है? पार्टियां इस निर्णय प्रक्रिया के दौरान खुद को कैसे प्रस्तुत करती हैं? दरअसल, इस पूरी प्रक्रिया को मार्केटिंग के उस सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है, जिसमें किसी उपभोक्ता के खरीदारी के फैसले को अलग-अलग चरणों में बांटकर समझा जाता है।
उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अनुसार, किसी भी खरीदारी के फैसले में पांच प्रमुख चरण होते हैं: जरूरत की पहचान, जानकारी की खोज, विकल्पों का मूल्यांकन, निर्णय लेना, और परिणाम के बाद की संतुष्टि। इनमें से अंतिम चरण, यानी परिणाम के बाद की संतुष्टि, एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे किसी सरकार के कामकाज के आधार पर ही मापा जा सकता है। लेकिन इसके पहले के चार चरणों का विश्लेषण अवश्य किया जा सकता है। यह विश्लेषण इसलिए अनोखा है क्योंकि भारतीय राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। आज राजनीतिक दल मतदाताओं को नीतियों, योजनाओं और वादों का एक 'पैकेज' पेश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई कंपनी अपने ग्राहकों को उत्पाद बेचने के लिए आकर्षक ऑफर देती है। चुनाव अब 'कॉर्पोरेट मॉडल' की तर्ज पर लड़े जा रहे हैं, जहां 'मार्केटिंग' एक प्रभावी हथियार बन चुकी है।
जरूरत की पहचान: 2014 के बाद भारतीय राजनीति में मतदाताओं की प्राथमिकताएं साफ़ तौर पर उभरकर सामने आई हैं। जनता एक स्थिर और मजबूत सरकार, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली सरकार, तेज़ी से बुनियादी ढांचा विकसित करने वाली सरकार, और सबसे महत्वपूर्ण, देश की युवा आबादी की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने वाली सरकार चाहती है। यदि हम भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को देखें, तो वे 2013 से ही इन सभी मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस लगातार अपने 'गोल पोस्ट' बदलती रही है और अक्सर ऐसे मुद्दे उठाती है, जो वास्तविक मतदाता की जरूरत से दूर होते हैं। चाहे वह अडानी-अंबानी पर हमले हों, संविधान खतरे में है जैसी बातें, या फिर प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले। यही बड़ा अंतर भाजपा के लिए आज एक वरदान साबित हुआ है। आज भाजपा देश के बड़े भूभाग पर इसलिए काबिज़ है, क्योंकि वह मतदाताओं की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं को सही मायनों में समझने में सफल रही है।
उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के मतदाताओं की सबसे बड़ी आवश्यकता स्थिरता और विकास थी। 2019 के बाद पहले ढाई साल तक महा विकास अघाड़ी सरकार के अस्थिर कार्यकाल और फिर शिवसेना और एनसीपी के विभाजन ने मतदाताओं को स्थिरता की अहमियत का अहसास कराया। दोनों गठबंधनों की रणनीतियों में स्पष्ट अंतर दिखा। महा विकास अघाड़ी यह मानकर चल रही थी कि लोकसभा चुनावों की तरह विधानसभा चुनावों में भी जनता उनके पक्ष में वोट करेगी। इसके विपरीत, महायुति का प्रचार अभियान, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, स्थिरता, डबल इंजन सरकार, और मजबूत नेतृत्व के संदेश पर केंद्रित था।
जानकारी की खोज: जब उपभोक्ता अपनी जरूरत को पहचान लेता है, तो अगला चरण होता है विकल्पों की जानकारी जुटाना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उपलब्ध विकल्पों का आकलन करता है। चुनावी संदर्भ में, यही वह समय होता है जब मतदाता विभिन्न पार्टियों के वादों, उनके नेतृत्व की क्षमता और गठबंधनों की ताकत का मूल्यांकन करते हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में और उससे पहले ही समझ लिया था कि सोशल मीडिया सूचना के लोकतांत्रीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है। आज भाजपा की सूचना प्रणाली इतनी व्यापक और गहरी है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही मिनटों में पूरे देश में बूथ स्तर तक किसी भी सूचना को पहुंचा सकता है। वहीं, कांग्रेस ने शुरू में इस शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। इसके विपरीत, भाजपा ने अपने नेताओं, पार्टी इकाइयों और मंचों की सोशल मीडिया उपस्थिति को हमेशा सुदृढ़ बनाए रखा।
Also Read- विशेष लेख: राष्ट्र-चिंतन- रोहिंग्या-बांग्लादेशी डेमोग्राफी रोकेंगी भाजपा की रफ्तार।
यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, जब मतदाता जानकारी जुटा रहा होता है, तो पार्टियां अपने संदेश को कैसे संप्रेषित करती हैं। भाजपा के पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्रभावशाली संदेशवाहक है, जो हमेशा अपनी बात को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ पहुंचाते हैं। दूसरी ओर, विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, कई बार अपने संदेश में भ्रमित नजर आते हैं।
विकल्पों का मूल्यांकन: यह वह चरण है जब उपभोक्ता अपने सामने मौजूद सभी विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण करता है और तय करता है कि कौन सा विकल्प उसकी जरूरतों और अपेक्षाओं को सबसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। चुनावी संदर्भ में, यही वह समय होता है जब मतदाता विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों, उनके नेताओं की छवि, और उनके वादों का आकलन करता है। अगर भाजपा की बात करें, तो वह हमेशा एक 'पूर्ण पैकेज' के साथ सामने आती है। इसमें सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं होती हैं, जो लाभार्थियों को सीधे जोड़ती हैं। "बटेंगे तो कटेंगे" जैसी स्पष्ट वैचारिक रेखाएं होती हैं। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर स्पष्ट राय होती है। प्रधानमंत्री मोदी जैसा करिश्माई और भरोसेमंद चेहरा, एक मजबूत संगठन, और एक मॉडल शासन—चाहे वह गुजरात का विकास मॉडल हो या यूपी का कानून-व्यवस्था मॉडल—भाजपा को एक समग्र और सशक्त विकल्प बनाता है।
इसके विपरीत, कांग्रेस के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है, जिसे वह पेश कर सके। खासकर राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपलब्धियां ऐसी नहीं हैं, जो मतदाताओं को आकर्षित कर सकें। कांग्रेस अक्सर वैचारिक रूप से भ्रमित पार्टी के रूप में दिखती है। राष्ट्रीय मुद्दों पर, जहां राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत होती है, कांग्रेस अक्सर 'वोट बैंक' के तर्क में उलझी नजर आती है। इसी वजह से जब मतदाता आज विकल्पों का मूल्यांकन करता है, तो उसे भाजपा बनाम कांग्रेस में भाजपा एक स्पष्ट और मजबूत विकल्प के रूप में नजर आती है। यही कारण है कि 10 साल के शासन के बाद भी भाजपा आज लोकसभा में उतनी सीटें जीत पाती है, जितनी पूरा विपक्ष मिलकर नहीं जीत सका।
निर्णय लेना: निर्णय लेना वह चरण है जब उपभोक्ता सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद आखिरी फैसला करता है। चुनावी परिदृश्य में, यह वह क्षण होता है जब मतदाता यह तय करता है कि वह अपना वोट किसे देगा। लेकिन, इस महत्वपूर्ण चरण में, सबसे अहम यह है कि पार्टियां अपने मतदाताओं को कैसे प्रेरित करती हैं और उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए क्या प्रयास करती हैं। अमित शाह की भाषा में कहें तो, "हमें सीट नहीं, बूथ जीतना है। अगर बूथ जीत गए, तो चुनाव हमारा।" भाजपा का संगठनात्मक ढांचा इस सिद्धांत पर पूरी तरह खरा उतरता है। आज भाजपा 'पन्ना प्रमुख' तक पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि हर कार्यकर्ता मतदाता सूची के एक पन्ने का प्रभारी होता है। यह जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष से लेकर एक साधारण कार्यकर्ता तक सभी निभाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पन्ना प्रमुख के रूप में काम करते हैं।
इसके विपरीत, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके पास अब ऐसा संगठनात्मक ढांचा ही नहीं है, जो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की प्रक्रिया को संभाल सके। देश के कई राज्यों में तो स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं हैं, बूथ अध्यक्ष तो दूर की बात है। यही अंतर भाजपा को कांग्रेस से बहुत आगे ले जाता है। जब मतदाता निर्णय लेने की प्रक्रिया में होता है, भाजपा का कैडर उसके लिए हर कदम पर उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में भाजपा ने एक अनूठा प्रयोग किया।
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, सुपर सीनियर सिटीजन (85 साल से अधिक उम्र) वाले मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को घर से ही डाक मतपत्र के जरिए वोट डालने का विकल्प मिलता है। भाजपा ने इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 3000-4000 ऐसे मतदाता होते हैं। इन वोटों का महत्व तब और बढ़ जाता है, जब किसी सीट का परिणाम महज 100-200 वोटों के अंतर से तय होना हो। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इन मतदाताओं तक पहुंचकर न केवल उन्हें मतदान प्रक्रिया में शामिल किया, बल्कि यह महसूस कराया कि कौन सी पार्टी उनके पास पहुंच रही है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा इन प्रक्रियाओं में हमेशा सफल रहती है। खासकर वहां, जहां कोई मजबूत क्षेत्रीय दल है और उसका अपना प्रभावशाली कैडर है, भाजपा पिछड़ जाती है। उदाहरण के लिए, झारखंड में मतदाताओं ने झामुमो का साथ दिया, क्योंकि हेमंत सोरेन ने आदिवासी अस्मिता, जल, जंगल, जमीन जैसे स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। उन्होंने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मइया योजना का बड़े पैमाने पर प्रचार किया, जिससे ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं का समर्थन मिला। इसके विपरीत, भाजपा ने अपना प्रचार अभियान अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर केंद्रित किया, जो झारखंड के स्थानीय मतदाताओं की प्राथमिकताओं से मेल नहीं खा सका।
इससे यह स्पष्ट होता है कि आज राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि केवल नाराजगी के भरोसे बैठकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। जरूरत है एक संपूर्ण तंत्र की, जो मतदाताओं की जरूरतों को समझे, अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से उन तक पहुंचाए, और उन्हें मतदान केंद्र तक लाने में सक्रिय भूमिका निभाए। ये समझना जरुरी है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव लड़ने के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। अब हर पार्टी को अपने पुराने तरीकों से बाहर निकलकर नई तैयारी करनी होगी।
What's Your Reaction?